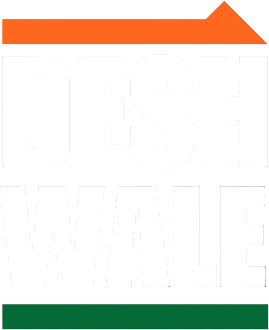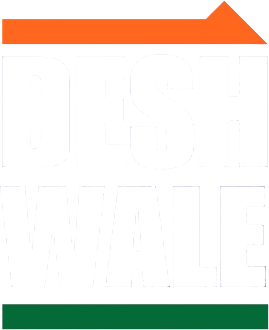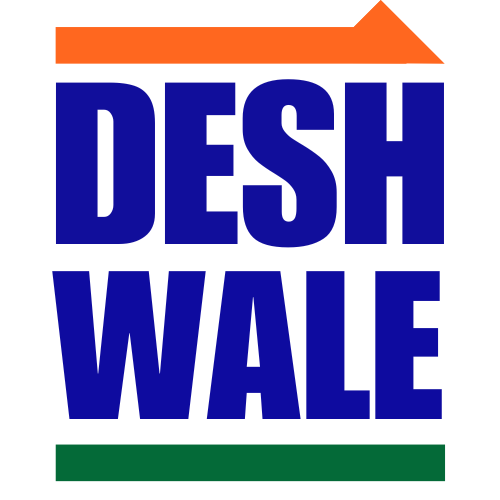हर सुबह जब मंदिर की घंटी बजती है, एक अलग ही सुकून दिल में उतरता है। मन खुद-ब-खुद शांत होने लगता है, जैसे किसी आंतरिक ऊर्जा ने हमारे भीतर प्रवेश कर लिया हो।
भारत में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होते; ये हमारी संस्कृति, परंपरा और आत्मिक शांति का केंद्र होते हैं। यहां घंटियों की गूंज, दीपक की लौ और मंत्रों की ध्वनि केवल कानों को नहीं, आत्मा को भी छू जाती है। ऐसे पवित्र स्थान पर हम कैसे जाते हैं, क्या पहनते हैं यह केवल एक बाहरी रूप नहीं, हमारी भीतरी भावना का भी प्रतिबिंब होता है।
आजकल देश के कई बड़े मंदिरों ने ड्रेस कोड लागू करना शुरू किया है। कुछ लोग इसे ज़रूरी कदम मानते हैं, जबकि कुछ इसे व्यक्तिगत आज़ादी पर रोक मानते हैं। पर इस विषय को समझने के लिए केवल “छूट या पाबंदी” के नजरिए से देखना पर्याप्त नहीं है। यह बहस केवल कपड़ों की नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, श्रद्धा और सामूहिक अनुशासन की है।
क्या एक पवित्र स्थान के लिए विशेष परिधान अपनाना हमारी आस्था को और गहराई नहीं देता? क्या धार्मिक स्थानों की गरिमा बनाए रखना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी है, या हमारी भी? यही सवाल इस लेख की आत्मा हैं, जिसे अब हम मिलकर समझते है –
धर्म और पोशाक: साथ चलते संस्कार
भारत में धर्म और परिधान का संबंध सदियों पुराना है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की जीवन शैली में भी शामिल रहा है।
- एक किसान जब खेत में उतरता है, तो वह भी गमछा या धोती पहनता है, क्यों? क्योंकि वो उसका काम करने का सम्मानजनक और व्यावहारिक पहनावा है।
- वैसा ही मंदिर में प्रवेश करते समय अगर हम विशेष वस्त्र पहनते हैं, तो वो सिर्फ परंपरा नहीं, एक मन:स्थिति बन जाती है, हम अपने दैनिक जीवन से अलग होकर ईश्वर से जुड़ने जा रहे हैं।
हिंदू धर्म में विशेष अवसरों पर साफ़, सादा और शुद्ध वस्त्र पहनना धर्मशास्त्रों में वर्णित है। सिख धर्म में गुरुद्वारा में सिर ढंकना, इस्लाम में मस्जिद में पूरी आस्तीन और ढके हुए शरीर के साथ जाना, और ईसाई धर्म में चर्च में सादगीपूर्ण ड्रेस – ये सब सिर्फ़ नियम नहीं हैं, श्रद्धा की भाषा हैं।
आज मंदिरों में ड्रेस कोड क्यों लागू हो रहे हैं?
कई बड़े मंदिर जैसे कि:
- सबरीमाला मंदिर : यहाँ पुरुष श्रद्धालुओं को लुंगी एवं शर्ट पहनकर जाना योग्य माना जाता है।
- सिद्धीविनायक मंदिर: यहाँ भी श्रद्धालुओं को सादे पारंपरिक वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है।
- मीनाक्षी अम्मन मंदिर : यहाँ विदेशी सैलानियों को भी अब ड्रेस कोड का पालन करना पड़ता है।
- पद्मनाभस्वामी मंदिर: यहाँ पुरुषों के लिए धोती या मुण्डू पहनना अनिवार्य है, और उन्हें शर्ट पहनने की अनुमति नहीं होती। महिलाओं को साड़ी, मुण्डुम नेरियाथुम पहनकर ही प्रवेश की अनुमति मिलती है
क्यों? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, “टूरिस्ट स्पॉट“ भी बन गए हैं। और इस बदलाव के साथ लोगों का पहनावा भी बदलने लगा। कैमरों के सामने ‘कूल’ दिखने के चक्कर में लोग भूलने लगे कि वो ईश्वर के घर में खड़े हैं, इंस्टाग्राम पर नहीं।
पहनावे और मानसिक अवस्था का संबंध
हम जैसा पहनते हैं, वैसा सोचते हैं। जब आप फॉर्मल मीटिंग में होते हैं, तो सूट-बूट में आपके हावभाव अपने आप गंभीर हो जाते हैं। उसी तरह, जब हम मंदिर में सादे, साफ और पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं, तो मन भी झुकता है। हम खुद को छोटा महसूस करते हैं, और ईश्वर के सामने झुकने का भाव बढ़ता है।
अगली पीढ़ी क्या सीख रही है?
आज का बच्चा बहुत सूझ-बूझ वाला है, लेकिन वह देख-देखकर ही सीखता है। अगर हम मंदिर में बिना सिर ढके, भड़काऊ या बहुत टाइट कपड़े पहनकर जाते हैं, तो उसे यह बात सामान्य लगने लगेगी। धीरे-धीरे मंदिर की मर्यादा उसकी समझ से बाहर हो जाएगी।
पर जब वह देखता है कि उसके माता-पिता मंदिर में धोती, साड़ी या सिर पर पल्लू लेकर जाते हैं, तो वह समझता है — “यह कोई आम जगह नहीं, यहां कुछ विशेष बात है।” और यही वह बात है जो संस्कार बनती है।
क्या ड्रेस कोड ज़रूरी या जबरदस्ती है?
ड्रेस कोड कोई ‘बैन’ नहीं है, यह एक सांस्कृतिक निवेदन है। जैसे कोई घर में मेहमान आता है और हम चाहते हैं कि वह जूते बाहर उतार दे; यह कोई अपमान नहीं, बल्कि घर की गरिमा बनाए रखने की अपील है।
वैसे ही मंदिर प्रशासन भी चाहता है कि श्रद्धालु जब आएं, तो उनका पहनावा उस माहौल को सम्मान दे, न कि उसमें खलल डाले।
दुनिया क्या कर रही है?
भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के धार्मिक स्थलों में ड्रेस कोड का पालन होता है:
- वेटिकन सिटी के चर्चों में स्कर्ट या बिना आस्तीन के कपड़ों में प्रवेश वर्जित है।
- मक्का-मदीना में हज के दौरान हलके रंगो के वस्त्र और पुरे शरीर को ढकना अनिवार्य है।
- थाईलैंड के बौद्ध मंदिरों में कंधे और घुटनों को ढकना ज़रूरी है।
तो फिर भारत में ऐसा होना कोई असामान्य बात नहीं बल्कि यह विश्व-परंपरा का हिस्सा है।
श्रद्धा का संवाद – सिर्फ़ शब्दों में नहीं, पोशाक में भी
जब हम मंदिर में जाते हैं, तो हम सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो क्या हमारे कपड़े भी उस भक्ति का हिस्सा नहीं हैं?
एक साड़ी पहनी महिला, एक धोती पहना पुरुष जब मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते है, तो वहाँ सिर्फ़ कपड़े नहीं होते, एक परंपरा चढ़ती है, एक संस्कृति प्रवेश करती है।
पहनावा बदलिए, भक्ति की गहराई बढ़ाइए
आधुनिकता का अर्थ यह नहीं कि हम सब कुछ पुराना छोड़ दें। बल्कि समझदारी यह है कि हम जो मूल्यवान है, उसे नई पीढ़ी तक ऐसे पहुँचाएं कि वे उसे गर्व से अपनाएं।
ड्रेस कोड पुराने जमाने की जंजीर नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए एक रास्ता है जो हमें अनुशासन, समानता और श्रद्धा सिखाता है।
तो अगली बार जब आप किसी मंदिर जाएं, एक बार शीश झुकाने से पहले यह ज़रूर सोचिए, “क्या मैं ईश्वर के सामने वैसे ही खड़ा हूँ, जैसे मुझे होना चाहिये?”