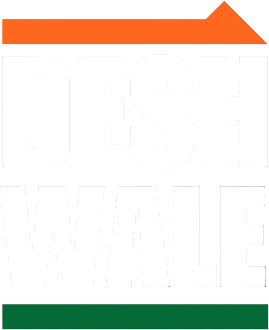भारत और चीन, एशिया के दो प्रमुख और सबसे तेजी से बढ़ते हुए देशों के रूप में हमेशा से एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन दोनों देशों का इतिहास और संस्कृति प्राचीन है, लेकिन 20वीं सदी में सीमा विवादों, राजनीतिक मतभेदों और वैश्विक शक्ति संघर्षों के कारण इन दोनों देशों के रिश्तों में जटिलताएँ आ गईं हैं। चीन का एक प्रतिस्पर्धी और चुनौतीपूर्ण रवैया, विशेष रूप से भारत के साथ, दोनों देशों के रिश्तों में एक महत्त्वपूर्ण अवरोध बनकर उभरा है।
इस लेख में, हम न केवल भारत-चीन के ऐतिहासिक संबंधों, सीमा विवाद और आर्थिक सहयोग का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, बल्कि चीन के प्रतिस्पर्धी रवैये और इसके परिणामस्वरूप द्विपक्षीय संबंधों पर होने वाले असर को भी समझेंगे।
भारत और चीन का ऐतिहासिक संबंध
भारत और चीन के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराना है। भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का प्रसार भारत से बाहर सर्वप्रथम चीन में ही हुआ था। भारतीय विचारधाराएँ, दर्शन और शिक्षा ने सर्वप्रथम चीन की संस्कृति पर ही गहरी छाप छोड़ी थी। प्राचीन काल में दोनों देशों ने एक-दूसरे से जमकर ज्ञान और संस्कृति का आदान-प्रदान किया था।
लेकिन 20वीं सदी में दोनों देशों के रिश्तों में बड़ा मोड़ आया, खासकर जब 1949 में चीन में माओत्से तुंग की सरकार बनी और भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जिससे भारत-चीन के रिश्तों में खटास आ गई। इसके बाद 1962 में सीमा विवाद के चलते भारत-चीन युद्ध हुआ, जिसने दोनों देशों के संबंधों में एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी।
सीमा विवाद और संघर्ष
भारत और चीन के बीच सबसे बड़ा विवाद उनकी साझा सीमा को लेकर है। यह सीमा लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी है, जिसे “लाइन्स ऑफ एक्चुअल कंट्रोल” (LAC) के नाम से जाना जाता है। इस सीमा पर कई क्षेत्रों को लेकर विवाद है, खासकर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन के इलाके।
1962 का युद्ध
भारत और चीन के रिश्तों में सबसे बड़ा मोड़ 1962 में आया जब चीन ने भारतीय क्षेत्रों पर हमला कर दिया था। यह युद्ध 34 दिनों तक चला और इसका परिणाम भारत की हार के रूप में हुआ। उस समय चीन ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। यह युद्ध न केवल दोनों देशों के रिश्तों में खटास लेकर आया, बल्कि भारत के जन-सामान्य के भीतर भी चीन के प्रति अविश्वास और डर को जन्म दिया।
1967 का भारत-चीन संघर्ष और इसके परिणाम
1967 में भारत और चीन के बीच हुआ दूसरा संघर्ष, जिसे नाथूला और चोला की झड़पें कहा जाता है, भारत-चीन संबंधों के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है। यह संघर्ष 1962 में हुए युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और तनाव का परिणाम था। इस संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि भारत ने 1962 के युद्ध से काफी कुछ सीखा था और अब वह अपनी सीमाओं की रक्षा में पूरी तरह से सक्षम था।
1967 के संघर्ष का माहौल 1962 के भारत-चीन युद्ध से उभरा था, जब चीन ने भारत को हराया और अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच सीमा विवादों ने और भी गहराई पकड़ ली थी। हालांकि, 1962 के युद्ध के बाद शांति कायम रखने के लिए दोनों देशों ने समझौतों की कई कोशिशें की, लेकिन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन के क्षेत्रों में तनाव बढ़ता ही रहा।
1967 में, इसी क्रम में नाथूला और चोला नामक स्थान पर घातक संघर्ष हुआ, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में और अधिक खटास आ गई। नाथूला, जो सिक्किम और तिब्बत के बीच स्थित एक महत्त्वपूर्ण पास है, इस संघर्ष का केंद्र बिंदु बना। यह एक महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्ग था। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच इस क्षेत्र में पहले भी अक्सर टकराव होते रहते थे। यहां दरअसल चीन ने भारतीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश की और अचानक भारतीय चौकियों पर हमला कर दिया था। लेकिन भारतीय सेना ने इसका कड़ा जवाब दिया और परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। भारतीय सेना ने चीनी सेना को अपनी स्थिति से खदेड़ा और उन्हें भारी नुकसान पहुँचाया। यह संघर्ष कुछ दिनों तक चला और अंत में एक संघर्ष विराम पर सहमति बनी। इस नाथूला संघर्ष में चीन को भारी नुकसान हुआ था। चीनी सैनिकों के लगभग 80 जवान मारे गए थे, जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या 70 के आसपास थी। यह संघर्ष वास्तव में भारत की शक्ति को प्रदर्शित करने वाला था। और भारत ने स्पष्ट रूप से यह भी संदेश दिया कि अब वह अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है।
चोला संघर्ष (अक्टूबर 1967)
नाथूला संघर्ष के बाद, अक्टूबर 1967 में चोला में भी एक छोटा-सा संघर्ष हुआ। यह संघर्ष भी सीमावर्ती इलाकों में चीन की घुसपैठ को लेकर हुआ था। परंतु भारतीय सेना ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और इस संघर्ष को कड़ा किया। चोला संघर्ष नाथूला की तुलना में छोटा था, लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को करारा जवाब दिया था। यह संघर्ष कुछ दिनों तक चला था और फिर युद्धविराम की स्थिति बन गई थी। भारत ने एक बार फिर यह साबित किया था कि वह अपनी सीमाओं की रक्षा में सक्षम है। हालांकि, चोला संघर्ष नाथूला जितना गंभीर नहीं था, फिर भी इसने चीन को यह संदेश दिया कि भारतीय सेना अब पहले से कहीं ज्यादा तैयार है।
1967 का संघर्ष भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण सैन्य विजय था। भारत ने यह साबित किया था कि उसने 1962 से बहुत कुछ सीखा है और अब वह अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह युद्ध भारत की सैन्य क्षमता के लिए एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था।
नाथूला और चोला संघर्षों ने भारत के मानचित्र पर सिक्किम की रणनीतिक महत्ता को उजागर किया था। यह क्षेत्र भारत और चीन के बीच एक महत्त्वपूर्ण सीमा है। भारतीय सेना ने तब भी इसे अपने नियंत्रण में बनाये रखने के लिए आवश्यक कदम उठाये थे और अब भी वह पूरी तरह से सजग और तत्पर रहती है। 1967 के संघर्ष के बाद, सिक्किम में भारतीय सेना की स्थिति को और मजबूत किया गया, और सिक्किम को 1975 में एक भारतीय राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया।
कुल मिलाकर 1967 के संघर्ष ने चीन को यह समझने पर मजबूर कर दिया कि भारत अब अपने सीमा क्षेत्रों की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। परिणामस्वरूप चीन ने नाथूला और चोला संघर्षों के बाद अपने सीमा नीतियों में बदलाव किये और भविष्य में भारत के खिलाफ आक्रामकता से बचने का प्रयास भी किया। हालांकि वह संघर्ष पूर्ण युद्ध में नहीं बदला था, लेकिन इसने दोनों देशों के बीच मनोबल में अवश्य गिरावट ला दी थी। फिर तो सीमा विवादों पर अनेकों बार चर्चा करने के बावजूद, दोनों देशों के रिश्ते उतने सहज नहीं हो पाये।
दोनों देशों ने सीमावर्ती क्षेत्र में शांति बनाये रखने की कोशिश अवश्य की, लेकिन कूटनीतिक दृष्टिकोण से दोनों देशों के रिश्ते लंबे समय तक तनावपूर्ण रहे। 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी का चीन दौरा हुआ था और दोनों देशों ने रिश्तों में सुधार के प्रयास भी किये थे, लेकिन 1967 का संघर्ष हमेशा दोनों देशों के रिश्तों में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में बना रहा।
चीन का प्रतिस्पर्धी रवैया
इस तरह चीन का रवैया अक्सर भारत के लिए चुनौतीपूर्ण और प्रतिस्पर्धी रहा है। सीमा पर संघर्षों के अलावा, चीन ने अपनी आक्रामक विदेश नीति और सैन्य-विस्तार की रणनीति के तहत कई बार भारत के क्षेत्रीय सुरक्षा हितों को खतरे में डाला है। चीन का तिब्बत पर कब्जा और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत विभिन्न देशों में निवेश, विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ आर्थिक और सैन्य गठजोड़, भारत के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। चीन के नेता, विशेष रूप से माओ ज़ेडॉन्ग और जिनपिंग ने कभी भी खुले तौर पर यह नहीं कहा कि वे भारत के साथ शांति चाहते हैं। उल्टा उनका रवैया अक्सर अपनी शक्ति और प्रभुत्व को बढ़ाने की ओर ही होता है। 2017 में डोकलाम विवाद और 2020 में गलवान घाटी की झड़प ने चीन के इसी प्रतिस्पर्धी रवैये को उजागर किया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2017 में कहा था, “हमारी सेना को अपनी स्थिति और अधिकारों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, ताकि कोई बाहरी ताकत हमें चुनौती न दे सके।” यह बयान भारत के लिए एक स्पष्ट चुनौती था और चीन के आक्रामक दृष्टिकोण का संकेत था।
आर्थिक संबंध और व्यापार
भारत और चीन दोनों ही दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ हैं और उनकी अर्थव्यवस्थाओं में तेज़ी से वृद्धि भी हो रही है। चीन और भारत के बीच आर्थिक संबंधों का इतिहास व्यापारिक दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच 2000 के दशक में व्यापार बढ़ा और चीन से सस्ते उत्पादों का आयात भारत में बढ़ा।
व्यापार घाटा
भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। 2020-21 में यह घाटा 50 बिलियन डॉलर से अधिक था। बीते वित्तवर्ष 202-25 में यह व्यापार घाटा तो और भी चिंताजनक स्तर पर पहुँच गया है। इस वर्ष भारत से चीन को कुल 11.48 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ है और जवाब में वहां से भारत में हुआ आयात 100 बिलियन डॉलर से भी अधिक रहा है। चीन से भारत को आयात होने वाले उत्पादों में इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, रसायन, और चिकित्सा उपकरण प्रमुख हैं। दूसरी ओर, भारत का निर्यात चीन को ज्यादातर कृषि उत्पादों, खनिजों, फार्मास्यूटिकल्स, और वस्त्रों से संबंधित है।
चीन का व्यापारिक उद्देश्य
चीन का व्यापारिक उद्देश्य अपनी ‘वर्डलैंड’ और ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ जैसी परियोजनाओं के माध्यम से वैश्विक प्रभुत्व स्थापित करना है। इन परियोजनाओं के तहत, चीन दुनियाभर में निवेश कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं भी शामिल हैं, जो भारत के लिए प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण बन रही हैं।
भारत का आत्मनिर्भरता लक्ष्य
भारत ने चीन से आयात में कमी लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को लागू किया है। इन पहलुओं के जरिए भारत ने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने और चीनी उत्पादों पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया है। इस तरह, भारत का उद्देश्य अपने व्यापार घाटे को कम करना और घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करना है।
चीन के प्रतिस्पर्धात्मक रवैये ने भारत-चीन संबंधों को कई बार तनावपूर्ण बना दिया है। सीमा विवाद, चीनी आक्रामकता, और पाकिस्तान जैसे देशों से चीन के गठजोड़ ने भारत को रणनीतिक दृष्टि से लगातार चुनौती दी है। 2020 के गलवान घाटी संघर्ष में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय जवानों पर हमला करना, भारत-चीन के संबंधों में एक नया मोड़ था, और इसने दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी को और बढ़ा दिया।
अर्थशास्त्र और सुरक्षा के बीच संतुलन
भारत को अपने आर्थिक विकास को बढ़ाने के साथ-साथ अपने सुरक्षा हितों की रक्षा करने की भी जरूरत है। यह इसलिए क्योंकि चीन के प्रतिस्पर्धी रवैये ने भारत को अपनी सैन्य और कूटनीतिक ताकत को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। परिणामस्वरूप भारत ने अपने रक्षा खर्चों में वृद्धि की है और समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा अंतरिक्ष क्षेत्र में भी अपनी शक्ति को बढ़ाया है।भारत-चीन के संबंधों का भविष्य
यदि दोनों देशों के नेतृत्व ने सही दिशा में कदम उठाए, तो भारत और चीन के बीच बेहतर और सामंजस्यपूर्ण संबंध संभव हो सकते हैं। चीन के प्रतिस्पर्धी रवैये को समझते हुए, भारत को अपनी रणनीतिक सोच को बढ़ाना होगा, ताकि वह न केवल अपने सुरक्षा हितों की रक्षा कर सके, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी अपनी स्थिति मजबूत बना सके।